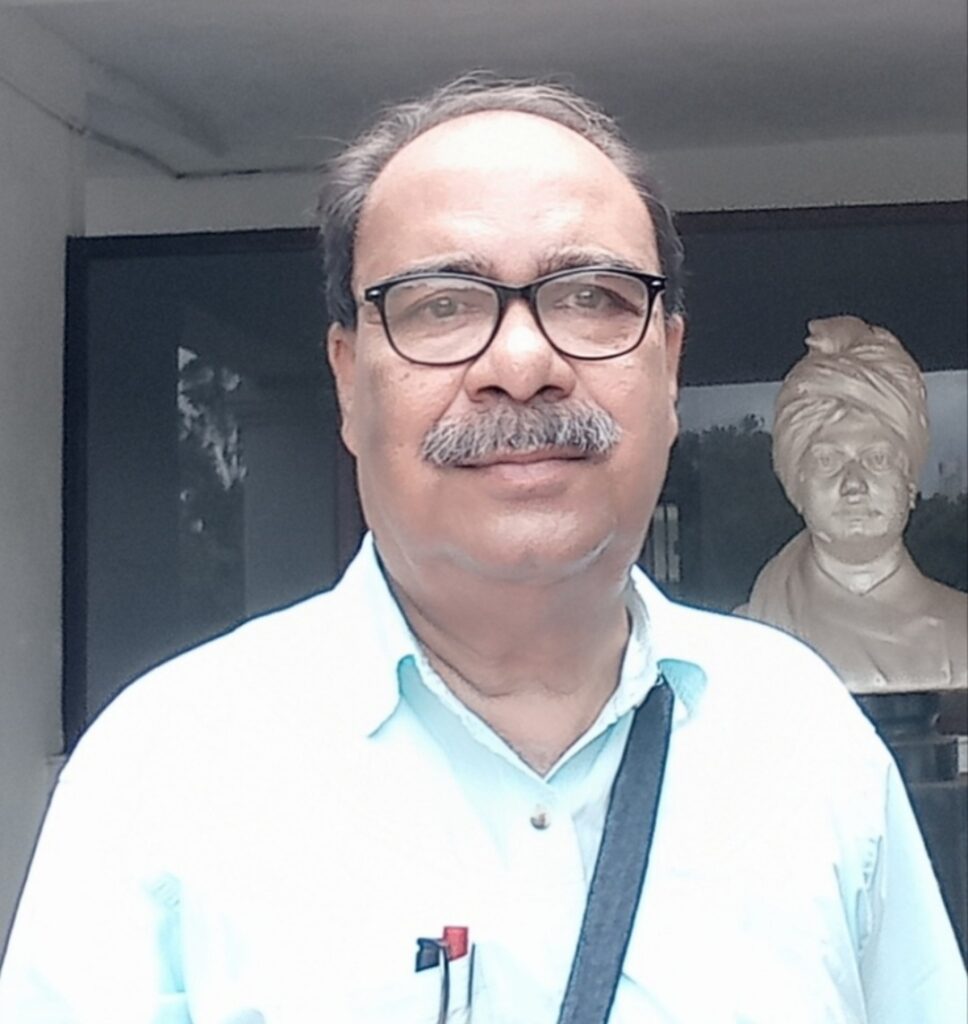आलेख: प्रेम की पोटली
आज प्रेम और स्नेह के लुप्त हो जाने की चर्चा बड़े जोरों पर है। डर लगता है की कहीं पर्यावरण बचाओ की तरह इसे भी एक नारा न बना दिया जाय।आजकल बहुत जगह स्टीकरों पर “मुस्कुराते रहें” चिपका देख रहा हूं, लेकिन लोगों के चेहरों पर तो सिर्फ तूफान है या फिर खोखली हंसी है।ऐसा न हो कि “चिपको आंदोलन” की तरह प्रेम और स्नेह की रक्षा के लिए कोई आगे आ जाए और फिर…………… नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं “चिपको आंदोलन” अथवा पर्यावरण की रक्षा का हिमायती नहीं हूं। दरअसल मैं चाहता हूं कि इन्सान और पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के बीच जो मौलिक अंतर है उसे बरकरार रखा जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि स्नेह और प्रेम जैसी भावनाएं घट रही हैं। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। यह अब भी यथावत है और उसी परिमाण में है क्योंकि इनका संबंध मनुष्य के शाश्वत स्वभाव से है। हां,अगर कुछ बदली है तो हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारा दृष्टिकोण नजरिया वगैरह।
यह सत्य है कि मुझको, तुमको, उसको, सबको एक न एक दिन सबकी पहचान हो ही जाती है। प्रेम कहां है? लेकिन कब ? जब हम अकेले में हों और अंतर्मन को टटोल रहे हों, तब। ऐसे कहां भीड़ में, आडंबर में, प्रेम खोजना भूसे में सुई तलाशने से भी अधिक दुष्कर है।
“प्रेम” आज भी एक पोटली का ही मोहताज है। प्रेम सुदामा का वह पोटली है जिसे “श्री कृष्ण” ने राजमहल के तमाम चकाचौंध के बीच भी ढूंढ निकाला था। इसीलिए तो वे योगिराज हैं। स्नेह की पोटली से पेट नहीं भरता। इससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। सुदामा के तंडुल से क्या “श्री कृष्ण” की भूख को स्वाद मिला था ? नहीं, आत्मा को। मुख के स्वाद के लिए तो राजमहल की खीर पूड़ी काफी थी।
आज के हर आदमी के सिर पर आडंबर का बड़ा सा टोकरा भले ही रखा हो, उसकी कांख में दबी हुई प्रेम और स्नेह की एक पोटली भी है।